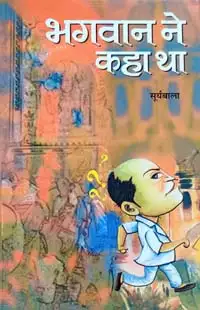|
कहानी संग्रह >> एक इन्द्रधनुष जुबेदा के नाम एक इन्द्रधनुष जुबेदा के नामसूर्यबाला
|
85 पाठक हैं |
|||||||
मानवीय संबंधों व प्रेम के गहरे अहसासों का वर्णन किया गया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
एक लंबे अन्तराल के बाद प्रस्तुत है प्रतिष्ठित कथाकार सूर्यबाला का पहला
कहानी-संग्रह ‘एक इन्द्रधनुषः जुबेदा के नाम’ जिसकी ‘रेस’, ‘निर्वासित’,
‘पलाश के फूल’ आदि सभी शुरूआती कहानियों में क्रमशः ‘सारिका’ और
‘धर्मयुग’ आदि स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ ही
प्रायः सभी आयु वर्ग के पाठकों और मर्मज्ञों का ध्यान खींचा था, उन्हें
अपने सम्मोहन में बाधा था।
तब से आज तक सूर्यबाला के कथा साहित्य का कैनवास गाँव से शहर-शहर से महानगर के साथ-साथ मध्य और उच्च वर्ग तक फैले रेंज के लिए जाना जाता है।
प्रारंभ से ही सूर्य बाला ने अपनी कहानियों के कत्थ और शिल्प की कोई सीमा नहीं बाँधी। बाजार के रुख से बेखबर वे माँग और सप्लाई वाले ट्रेंड की अनसुनी करती रही। समायिकता के ऊपरी और सतही दबाव भी उन्हें नहीं भरमा पाए। लेकिन उनकी प्रत्येक रचना अपने समय का विद्रूपता और व्यक्ति की संवेदना को तेजी से निगलती व्यावसायिकता का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी चाहे वर्ग भेद के ध्रुवांतों की हो (लाल पलाश...) चाहे आज की अंधी दौड़ (रेस) और चाहे रीतते मानवीय संबंधों (निर्वासित) की या प्रेम के गहरे अहसासों की हर रचना का समय की समग्रता में प्रवेश करने की कोशिश करती है।
पढ़नेवालों की हमेशा इन कहानियों की प्रतीक्षा शायद इसीलिए रहती है, क्योंकि इनके पात्रों में वे स्वयं अपने को ढूँढ़ पाते हैं। बीस बरस पहले लिखी जाकर भी ये कहानियाँ आज तक पुरानी नहीं पड़ीं।
तब से आज तक सूर्यबाला के कथा साहित्य का कैनवास गाँव से शहर-शहर से महानगर के साथ-साथ मध्य और उच्च वर्ग तक फैले रेंज के लिए जाना जाता है।
प्रारंभ से ही सूर्य बाला ने अपनी कहानियों के कत्थ और शिल्प की कोई सीमा नहीं बाँधी। बाजार के रुख से बेखबर वे माँग और सप्लाई वाले ट्रेंड की अनसुनी करती रही। समायिकता के ऊपरी और सतही दबाव भी उन्हें नहीं भरमा पाए। लेकिन उनकी प्रत्येक रचना अपने समय का विद्रूपता और व्यक्ति की संवेदना को तेजी से निगलती व्यावसायिकता का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी चाहे वर्ग भेद के ध्रुवांतों की हो (लाल पलाश...) चाहे आज की अंधी दौड़ (रेस) और चाहे रीतते मानवीय संबंधों (निर्वासित) की या प्रेम के गहरे अहसासों की हर रचना का समय की समग्रता में प्रवेश करने की कोशिश करती है।
पढ़नेवालों की हमेशा इन कहानियों की प्रतीक्षा शायद इसीलिए रहती है, क्योंकि इनके पात्रों में वे स्वयं अपने को ढूँढ़ पाते हैं। बीस बरस पहले लिखी जाकर भी ये कहानियाँ आज तक पुरानी नहीं पड़ीं।
सूर्यबाला और रचनाशीलता
आज कहानी जिंदगी से जितनी जुड़ गई है, उतनी साहित्य की कोई और विधा नहीं
जुड़ पाई। कविता बिंबों में उलझकर वक्त से कट गई। नाटक एक तो लिखे ही कम
गए हैं और जो लिखे गए हैं उनमें से अधिकांश या तो ऐतिहासिक तिलिस्म में खो
गए हैं या प्रदर्शन की चकाचौंध में-और जो शेष रहे हैं वे पर्याप्त नहीं
हैं। बचती है कहानी। कहानी ने अपनी यात्रा बड़ी तेजी से तय की है। वह तेजी
आज के यांत्रिक युवक की तेजी भी है और समाज की बदलती हुई मान्यताओं की भी।
जीवन-मूल्य जिस तेजी से बदले हैं कहानी की गतिशीलता भी उतनी ही बढ़ी है।
इस गति के कारण आज की कहानी अपने वक्त से एकात्म होकर चल सकी है।
कहा जाता है कि विज्ञान ने दुनिया छोटी कर दी है, दूरियाँ कम कर दी हैं; लेकिन यह कमी भौगोलिक दूरियों में आई है; वैचारिकता, मानसिकता और रचनाशीलता की दूरी कहानी ने कम की है। आज विश्व के बहुत बड़े भाग का आदमी लगभग एक सी स्थितियों में साँस ले रहा है। सांस्कृतिक संकट, आत्मिक उलझनें, आर्थिक तनाव, राजनीतिक, उठा-पटक और वैचारिक विक्षोभ का प्रभाव दुनिया के हर आदमी पर करीब-करीब एक सा ही पड़ा है। यही कारण है कि दुनिया के हर बुद्धिजीवी, विशेषतः कहानीकार की सोच और अहसास लगभग एक जैसा ही है। हम एक-दूसरे की तकलीफ संत्रास और त्रासदी के अधिक करीब आए हैं।
पहले के साहित्य में दर्शन, विचारधारा और वैशिष्ट्य का सामान्यीकरण होता था; लेकिन आज की कहानियों में संपूर्ण जिंदगी और जिंदगी की सच्चाईयों का सामान्यीकरण हुआ है। यह अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। आज की कहानी की यही उपलब्धि है। इसमें किसी एक का नहीं, सही सोच के सभी रचनाधर्मियों का योगदान है।
सूर्यबाला का यह कहानी-संग्रह भी एक सोच की एक कड़ी है। इसमें नौ कहानियाँ हैं और सब में भाषा शिल्प व कथ्य की विविधता है, लेकिन इनका वैचारिक धरातल एक है। इनकी सोच का सिलसिला कहीं टूटा नहीं है। यही सिलसिला सूर्यबाला को सुलझे हुए रचनाकारों की श्रेणी में ले आता है।
इन कहानियों में जहाँ एक ओर संबंधों या रिश्तों का खोखलापन है, वहीं स्वार्थ के संकीर्ण दायरों का लेखा-जोखा भी है। कहीं-कहीं कहानियों में एक ठंडापन और ठहराव सा लगता है; लेकिन वह ठंडापन और ठहराव हार जाने या थक जाने का नहीं; परिस्थितियों, मजबूरियों और विक्षोभों का है और इसीलिए उसे नकारा नहीं जा सकता। इन कहानियों में हालात से जूझते हुए पात्र व्यवस्था के यथास्थितिवाद के मजबूत जाल में फँस गए हैं और उससे मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं।
‘निर्वासित’ के माता-पिता को नई पीढ़ी ने नहीं, उसके आर्थिक तनावों की मजबूरियों ने निरीह बनाया है।
‘व्याभिचार’ की नारी अपनी ही द्वंद्वात्मक मानसिकता की शिकार हो गई है और मांसलता के तिलिस्म को तोड़ने की असफल कोशिश कर रही है ‘रेस’ का व्यक्ति गलत महत्त्वाकांक्षा का शिकार है। सुलह की आर्थिक विषमताएँ आदमी को समझौतावादी बनने के लिए मजबूर कर रही हैं। ‘दरारें’ वर्गीय संघर्ष की कहानी है, जिसमें जख्मों की गारंटी होते हुए भी लड़ाई जारी रखने की मजबूरी है; क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपनी उपस्थिति का अहसास नहीं खोना चाहता। ‘अविभाज्य’ के नारी और पुरुष पात्र अपने अतीत से जुड़े रहकर अपनी मानसिकता का आधार खोजते हैं। यही खोज उन्हें एक-दूसरे के करीब बनाए हुए है।
वैचारिकता की दृष्टि से ‘समान सतहें’ इस संग्रह की सबसे अधिक सशक्त कहानी है। दो भिन्न स्वभाव के व्यक्ति तंगहाली और आर्थिक मजबूरियों के कारण एक ही सतह पर खड़े हैं। एक ही सतह पर खड़े होने का अहसास आज के आदमी का सही अहसास है।
आज का आदमी अपने छोटे-छोटे स्वार्थों और मानसिक संकीर्णताओं के कारण कितना कायर हो गया है, इसका अंदाज हाँ लाल पलाश के फूल सिर्फ अग्निवर्णी हैं, अग्निधर्मी नहीं।
इस संग्रह की शीर्षक कहानी एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम मुख्यतः एक माहौल की कहानी है। इसमें एक पिता का दर्द तंगहाली की लाचारी ने उभारा और बढ़ाया है। इस कहानी में हालाँकि कुछ भावुकता आ गई है; लेकिन वह भावुकता पुरानी बँगला कहानी का ‘सेंटीमेंटलिज्म’ नहीं है।
सारी कहानियों ने मिलकर इस संग्रह की एक स्पष्ट तसवीर उभारी है। वह तसवीर अपने वक्त की है, आज के आदमी की है। आज की कहानी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह किसी भी वर्जना को अस्वीकार करती है। वह सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ती, उसे फेस करती है। सच्चाई को रँगकर पेश करना बेईमानी है, सामाजिक न्याय के मार्ग में भुलावा पैदा करना है। इससे किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। रँगी-पुती सच्चाई आज का सौंदर्य बोध नहीं, सौंदर्य विकृति है। मुझे खुशी है कि सूर्यबाला ने अपने आपको इस सौंदर्य विकृति से बचाया है। सूर्यबाला की कहानियाँ वक्त की चिंतनधारा से कटी नहीं हैं, यही इनकी जीवनगत प्रामाणिकता है। हिंदी कथा-जगत् में सूर्यबाला की उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण हैं और मैं उनकी रचनाशीलता की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त हूँ।
कहा जाता है कि विज्ञान ने दुनिया छोटी कर दी है, दूरियाँ कम कर दी हैं; लेकिन यह कमी भौगोलिक दूरियों में आई है; वैचारिकता, मानसिकता और रचनाशीलता की दूरी कहानी ने कम की है। आज विश्व के बहुत बड़े भाग का आदमी लगभग एक सी स्थितियों में साँस ले रहा है। सांस्कृतिक संकट, आत्मिक उलझनें, आर्थिक तनाव, राजनीतिक, उठा-पटक और वैचारिक विक्षोभ का प्रभाव दुनिया के हर आदमी पर करीब-करीब एक सा ही पड़ा है। यही कारण है कि दुनिया के हर बुद्धिजीवी, विशेषतः कहानीकार की सोच और अहसास लगभग एक जैसा ही है। हम एक-दूसरे की तकलीफ संत्रास और त्रासदी के अधिक करीब आए हैं।
पहले के साहित्य में दर्शन, विचारधारा और वैशिष्ट्य का सामान्यीकरण होता था; लेकिन आज की कहानियों में संपूर्ण जिंदगी और जिंदगी की सच्चाईयों का सामान्यीकरण हुआ है। यह अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। आज की कहानी की यही उपलब्धि है। इसमें किसी एक का नहीं, सही सोच के सभी रचनाधर्मियों का योगदान है।
सूर्यबाला का यह कहानी-संग्रह भी एक सोच की एक कड़ी है। इसमें नौ कहानियाँ हैं और सब में भाषा शिल्प व कथ्य की विविधता है, लेकिन इनका वैचारिक धरातल एक है। इनकी सोच का सिलसिला कहीं टूटा नहीं है। यही सिलसिला सूर्यबाला को सुलझे हुए रचनाकारों की श्रेणी में ले आता है।
इन कहानियों में जहाँ एक ओर संबंधों या रिश्तों का खोखलापन है, वहीं स्वार्थ के संकीर्ण दायरों का लेखा-जोखा भी है। कहीं-कहीं कहानियों में एक ठंडापन और ठहराव सा लगता है; लेकिन वह ठंडापन और ठहराव हार जाने या थक जाने का नहीं; परिस्थितियों, मजबूरियों और विक्षोभों का है और इसीलिए उसे नकारा नहीं जा सकता। इन कहानियों में हालात से जूझते हुए पात्र व्यवस्था के यथास्थितिवाद के मजबूत जाल में फँस गए हैं और उससे मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं।
‘निर्वासित’ के माता-पिता को नई पीढ़ी ने नहीं, उसके आर्थिक तनावों की मजबूरियों ने निरीह बनाया है।
‘व्याभिचार’ की नारी अपनी ही द्वंद्वात्मक मानसिकता की शिकार हो गई है और मांसलता के तिलिस्म को तोड़ने की असफल कोशिश कर रही है ‘रेस’ का व्यक्ति गलत महत्त्वाकांक्षा का शिकार है। सुलह की आर्थिक विषमताएँ आदमी को समझौतावादी बनने के लिए मजबूर कर रही हैं। ‘दरारें’ वर्गीय संघर्ष की कहानी है, जिसमें जख्मों की गारंटी होते हुए भी लड़ाई जारी रखने की मजबूरी है; क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपनी उपस्थिति का अहसास नहीं खोना चाहता। ‘अविभाज्य’ के नारी और पुरुष पात्र अपने अतीत से जुड़े रहकर अपनी मानसिकता का आधार खोजते हैं। यही खोज उन्हें एक-दूसरे के करीब बनाए हुए है।
वैचारिकता की दृष्टि से ‘समान सतहें’ इस संग्रह की सबसे अधिक सशक्त कहानी है। दो भिन्न स्वभाव के व्यक्ति तंगहाली और आर्थिक मजबूरियों के कारण एक ही सतह पर खड़े हैं। एक ही सतह पर खड़े होने का अहसास आज के आदमी का सही अहसास है।
आज का आदमी अपने छोटे-छोटे स्वार्थों और मानसिक संकीर्णताओं के कारण कितना कायर हो गया है, इसका अंदाज हाँ लाल पलाश के फूल सिर्फ अग्निवर्णी हैं, अग्निधर्मी नहीं।
इस संग्रह की शीर्षक कहानी एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम मुख्यतः एक माहौल की कहानी है। इसमें एक पिता का दर्द तंगहाली की लाचारी ने उभारा और बढ़ाया है। इस कहानी में हालाँकि कुछ भावुकता आ गई है; लेकिन वह भावुकता पुरानी बँगला कहानी का ‘सेंटीमेंटलिज्म’ नहीं है।
सारी कहानियों ने मिलकर इस संग्रह की एक स्पष्ट तसवीर उभारी है। वह तसवीर अपने वक्त की है, आज के आदमी की है। आज की कहानी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह किसी भी वर्जना को अस्वीकार करती है। वह सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ती, उसे फेस करती है। सच्चाई को रँगकर पेश करना बेईमानी है, सामाजिक न्याय के मार्ग में भुलावा पैदा करना है। इससे किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। रँगी-पुती सच्चाई आज का सौंदर्य बोध नहीं, सौंदर्य विकृति है। मुझे खुशी है कि सूर्यबाला ने अपने आपको इस सौंदर्य विकृति से बचाया है। सूर्यबाला की कहानियाँ वक्त की चिंतनधारा से कटी नहीं हैं, यही इनकी जीवनगत प्रामाणिकता है। हिंदी कथा-जगत् में सूर्यबाला की उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण हैं और मैं उनकी रचनाशीलता की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त हूँ।
-कमलेश्वर
कहानी से पहले : आप और मैं
जिंदगी को जय-पराजय और कशमकशों के बीच हँसते-खिलखिलाते हुए, पूरी
जिंदादिली से जीनेवाली मैं अकसर भीड़ छँटने के बाद बेहद खामोश हो जाती
हूँ। मेरे भीतर तेजी से एक सन्नाटा खिंचने लगता है-और तब इन एकाकी क्षणों
में मेरी खामोशी बोलती है-इन कहानियों के रूप में मंत्रबिद्ध-सी उतनी देर
के लिए मैं बाहर भीतर एकदम बदल जाती हूँ; लेकिन सन्नाटा टूटने के बाद फिर
वही कशमकश और बेशर्म हँसी।
बस, अपने इन्हीं क्षणों का एक अति सामान्य उपहार है-यह संग्रह। पत्र-पत्रिकाओं की छत्रच्छाया में प्रकाशित होने में और सीधे अपने पाठकों के सामने आकर खड़े हो जाने में काफी अंतर महसूस हो रहा है। अधिक दायित्व के साथ अधिक आत्मीय-भाव का भी। पत्र-पत्रिकाओं में जब ये कहानियाँ प्रकाशन के लिए गई थीं तब मैं स्वयं, पत्रिका संपादक आदि भी प्रमुख थे; पर संग्रह के समय मेरे सामने केवल आप हैं-मेरे सहृदय ईमानदार पाठक। शायद इसलिए अपने इस प्रथम संग्रह के लिए मैंने विशेष रूप से वे ही कहानियाँ चुनी हैं, जो पाठकों के द्वारा विशेष रूप से पसंद की गई थीं। साथ ही उनकी एक सहज जिज्ञासा को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक कहानी के साथ उसकी मूल प्रेरणा या अंतःस्रोत को लेकर एक छोटा सा आत्मकथ्य भी रख दिया गया है। ‘सारिका’ में प्रकाशित मेरी कहानी ‘गौरा गुनवंती’ को लेकर कितने ही पाठकों ने मुझसे प्रकारांतर से एक ही सवाल पूछा था-‘गौरा आपको कहाँ मिली ?...इसमें कितना यथार्थ है, कितनी कल्पना आदि.....’ यों भी प्रायः सभी लेखकों की कहानियों से पाठकों को यह जिज्ञासा रहती ही है।
कहानियों के चयन की दृष्टि से संग्रह की एक और विशेषता है, वह है कथ्य और भाषा शिल्प के वैविध्य की, जिसमें कहीं अनुराग के लाल पलाश फूल रहे हैं तो कहीं अवसाद के हरसिंगार, कहीं नारी के अंदरूनी तिलिस्म (व्यभिचार) की गुलाबी डोरियाँ टूट रही हैं तो कहीं वृद्ध मानसिकता क्रौंच वध की पीड़ा से तड़प रही है (निर्वासित), कहीं हार की सुलह, है, कहीं जीत की विडंबना (रेस) कहीं अतीत का व्यामोह, कहीं वर्तमान की विसंगतियाँ और कहीं भविष्य के इंद्रधनुष टूटकर आसमान से जमीन पर गिरते हुए....
भाषा-शिल्प की दृष्टि से भी कहानियों के अनुरूप ही कहीं उच्च-मध्य वर्ग का अंग्रेजी दाँ लटका, कहीं नारी मानसिकता के साथ लिपटी काव्यात्मक शैली, कहीं अर्थतंत्र में पिसते यथार्थ के अनुरूप निर्मम तटस्थ, अनलंकृत सपाट शिल्प और कहीं मुसलिम संस्कृति के माहौल को उजागर करनेवाले प्रचलित उर्दू शब्द।
प्रायः लेखिकाओं के लेखन को घर-परिवारी, सेक्स संबंधों एवं दांपत्य-कुंठा तक ही सीमित मानने के साथ-साथ ऐसे ही कथ्यों की पुनरावृत्ति के भी आरोप लगाए जाते हैं। यद्यपि यह सभी लेखिकाओं के लिए सच नहीं, साथ ही प्रतिवादी कथनों के रूप में बहुत से अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तथापि मुझे संतोष है कि इस दृष्टि से मैंने अपने कथ्यों में कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उठाया हुआ कदम सार्थक कितना रहा, नहीं जानती।
कृति के आरंभ में वंदना की रीति किंचित् पुरानी पड़ गई है, किंतु मेरे लिए तो ऋण और आभार में नमित हो जाने के लिए यह एक जन्म संभवतः पर्याप्त नहीं, क्योंकि यह दायरा बहुत बचपन से सँवारने प्रेरणा, देनेवाले गुरुजनों से लेकर अब तक के अभिन्न हितचिंतकों एवं निस्स्वार्थ स्नेहिल भाव से संरक्षण, सम्मति एवं सहयोग देनेवाले आत्मीयों तक विस्तृत है। इतना ही क्यों, प्रकारांतर से जाने-अनजाने मेरी कहानियों में अपनी-अपनी भूमिका निभा जानेवाले पात्र भी मेरे लिए उतने ही अभिनंदनीय हैं। काश, मेरे शब्द गोस्वामी की भाँति वंदना की मर्यादा एवं सामर्थ्य ग्रहण कर पाते !
अंत में एक विवश कृतज्ञता पति के प्रति भी-जो करते-धरते तो कुछ नहीं-हाँ, अपनी निंदा, लथाड़ और फटकार के माध्यम से आकाश तक भटकते, डाँवाडोल होते मेरे मन को धरती पर ला मेरे आँगन की सीमा समझा देते हैं। कबीरदासजी की बात मान ली। निंदक के लिए कुटी भी नहीं छवानी पड़ी।
बस, काँच के इन्हीं रंग बिरंगे मनकों से आपका अभिनंदन है। भविष्य में सचमुच कुछ मूल्यवान् दे पाने की आकांक्षा एवं विश्वास के साथ-
बस, अपने इन्हीं क्षणों का एक अति सामान्य उपहार है-यह संग्रह। पत्र-पत्रिकाओं की छत्रच्छाया में प्रकाशित होने में और सीधे अपने पाठकों के सामने आकर खड़े हो जाने में काफी अंतर महसूस हो रहा है। अधिक दायित्व के साथ अधिक आत्मीय-भाव का भी। पत्र-पत्रिकाओं में जब ये कहानियाँ प्रकाशन के लिए गई थीं तब मैं स्वयं, पत्रिका संपादक आदि भी प्रमुख थे; पर संग्रह के समय मेरे सामने केवल आप हैं-मेरे सहृदय ईमानदार पाठक। शायद इसलिए अपने इस प्रथम संग्रह के लिए मैंने विशेष रूप से वे ही कहानियाँ चुनी हैं, जो पाठकों के द्वारा विशेष रूप से पसंद की गई थीं। साथ ही उनकी एक सहज जिज्ञासा को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक कहानी के साथ उसकी मूल प्रेरणा या अंतःस्रोत को लेकर एक छोटा सा आत्मकथ्य भी रख दिया गया है। ‘सारिका’ में प्रकाशित मेरी कहानी ‘गौरा गुनवंती’ को लेकर कितने ही पाठकों ने मुझसे प्रकारांतर से एक ही सवाल पूछा था-‘गौरा आपको कहाँ मिली ?...इसमें कितना यथार्थ है, कितनी कल्पना आदि.....’ यों भी प्रायः सभी लेखकों की कहानियों से पाठकों को यह जिज्ञासा रहती ही है।
कहानियों के चयन की दृष्टि से संग्रह की एक और विशेषता है, वह है कथ्य और भाषा शिल्प के वैविध्य की, जिसमें कहीं अनुराग के लाल पलाश फूल रहे हैं तो कहीं अवसाद के हरसिंगार, कहीं नारी के अंदरूनी तिलिस्म (व्यभिचार) की गुलाबी डोरियाँ टूट रही हैं तो कहीं वृद्ध मानसिकता क्रौंच वध की पीड़ा से तड़प रही है (निर्वासित), कहीं हार की सुलह, है, कहीं जीत की विडंबना (रेस) कहीं अतीत का व्यामोह, कहीं वर्तमान की विसंगतियाँ और कहीं भविष्य के इंद्रधनुष टूटकर आसमान से जमीन पर गिरते हुए....
भाषा-शिल्प की दृष्टि से भी कहानियों के अनुरूप ही कहीं उच्च-मध्य वर्ग का अंग्रेजी दाँ लटका, कहीं नारी मानसिकता के साथ लिपटी काव्यात्मक शैली, कहीं अर्थतंत्र में पिसते यथार्थ के अनुरूप निर्मम तटस्थ, अनलंकृत सपाट शिल्प और कहीं मुसलिम संस्कृति के माहौल को उजागर करनेवाले प्रचलित उर्दू शब्द।
प्रायः लेखिकाओं के लेखन को घर-परिवारी, सेक्स संबंधों एवं दांपत्य-कुंठा तक ही सीमित मानने के साथ-साथ ऐसे ही कथ्यों की पुनरावृत्ति के भी आरोप लगाए जाते हैं। यद्यपि यह सभी लेखिकाओं के लिए सच नहीं, साथ ही प्रतिवादी कथनों के रूप में बहुत से अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तथापि मुझे संतोष है कि इस दृष्टि से मैंने अपने कथ्यों में कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उठाया हुआ कदम सार्थक कितना रहा, नहीं जानती।
कृति के आरंभ में वंदना की रीति किंचित् पुरानी पड़ गई है, किंतु मेरे लिए तो ऋण और आभार में नमित हो जाने के लिए यह एक जन्म संभवतः पर्याप्त नहीं, क्योंकि यह दायरा बहुत बचपन से सँवारने प्रेरणा, देनेवाले गुरुजनों से लेकर अब तक के अभिन्न हितचिंतकों एवं निस्स्वार्थ स्नेहिल भाव से संरक्षण, सम्मति एवं सहयोग देनेवाले आत्मीयों तक विस्तृत है। इतना ही क्यों, प्रकारांतर से जाने-अनजाने मेरी कहानियों में अपनी-अपनी भूमिका निभा जानेवाले पात्र भी मेरे लिए उतने ही अभिनंदनीय हैं। काश, मेरे शब्द गोस्वामी की भाँति वंदना की मर्यादा एवं सामर्थ्य ग्रहण कर पाते !
अंत में एक विवश कृतज्ञता पति के प्रति भी-जो करते-धरते तो कुछ नहीं-हाँ, अपनी निंदा, लथाड़ और फटकार के माध्यम से आकाश तक भटकते, डाँवाडोल होते मेरे मन को धरती पर ला मेरे आँगन की सीमा समझा देते हैं। कबीरदासजी की बात मान ली। निंदक के लिए कुटी भी नहीं छवानी पड़ी।
बस, काँच के इन्हीं रंग बिरंगे मनकों से आपका अभिनंदन है। भविष्य में सचमुच कुछ मूल्यवान् दे पाने की आकांक्षा एवं विश्वास के साथ-
-सूर्यबाला
समान सतहें
आज से दस-ग्यारह वर्ष पूर्व उस छह फुटे, दबंग व्यक्ति का रोब-दाब देखकर
दंग रह गई थी। अच्छी सरकारी नौकरी, चपरासी, नौकर और ढेर से उछलते कूदते
बच्चे-जिनमें अधिकतर लड़कियाँ होने पर भी कभी उसके चेहरे पर शिकन नहीं
देखी। गरूर में लिपटी आवाज, रुआब से तनी गर्दन.....और इतने सालों बाद जो
उन्हें देखा-क्या ये वही थे ? पायरिया की तकलीफ से निकलवा दिए गए दाँतों
की वजह से पोपला मुँह, झुकी गरदन और माथे पर डेर सी सिलवटें....सभी
लड़कियाँ जैसे एक साथ ही खड़ी हो गई थीं....नौकर-चाकर, सरकारी बँगले और
रोब-दाब से हीन उनकी रिटायर्ड, तलछट सी जिंदगी। उतने सालों पहले के चमकते
साफ परदे अब भी कहीं-कहीं मैले बदरंग-से झूल रहे थे।
किशोर लड़का बार-बार साइकिल से आता-जाता हमारी आवभगत की सामग्री जुटाने के लिए दौड़ धूप कर रहा था....और गुल्लक ? शायद अपने ही घर कभी बहुत जरूरत पर किसी बच्चे का टूटा था और चुप रह जाने पर भी उस बच्चे की मूक वेदना ने मुझे इस कहानी की सतह पर खड़ा कर दिया था।
किशोर लड़का बार-बार साइकिल से आता-जाता हमारी आवभगत की सामग्री जुटाने के लिए दौड़ धूप कर रहा था....और गुल्लक ? शायद अपने ही घर कभी बहुत जरूरत पर किसी बच्चे का टूटा था और चुप रह जाने पर भी उस बच्चे की मूक वेदना ने मुझे इस कहानी की सतह पर खड़ा कर दिया था।
लेखिका
मैंने झिझकते हुए कुंडा खटखटाया। दरवाजा उन्होंने ही खोला। मुझे देखते हुए
एक लमहे को ‘कहिए, किसको चाहते हैं’ वाले पसोपेश में पड़े
रहे; पर मेरे नाम बताते ही, अरे आप ! आओ आओ, अंदर आओ’ कहकर
उन्होंने पूरा दरवाजा खोल दिया।
मैं खुद उनसे ज्यादा परोपेश में था। दरअसल, ऐसी नाजुक रिश्तेदारी में आना ही नहीं चाहता था, पर मंजु ने बहुत जोर डाला था, ‘चाचा को पता चलेगा तो कितना बुरा मानेंगे ! तुमने असल में उन्हें शादी पर थोड़ी ही देर को देखा है न, उनका स्वभाव नहीं जानते। बहुत ही खुशमिजाज आदमी हैं। सारा समय हँसते-हँसाते चुटकुले लतीफे सुनाते घर बाहर गुलजार किए रहते हैं। बचपन में हम सब पूरी गरमी की छुट्टियाँ चाचा के पास ही तो बिताते थे। बच्चों से उन्हें बेहद प्यार था। उनके बच्चों में तब केवल रानी थी। ओह कितना मजा आता था कभी कंधे पर बैठाकर घुमाते, कभी सब बच्चों को इकट्ठा कर ‘अकल गुम्म-अकल गुम्म’ का खेल खेलते। मैं बहुत मोटी थी न, दोनों गाल फूले रहते, सो अपना भी गाल फुलाकर ‘कुंडा लोगी कि गगरी’ कहकर चिढ़ाते उनके रहते कोई बच्चा रो नहीं सकता था। हमारी सारी जिदें पूरी की जातीं। हमें अपने घर से कहीं ज्यादा अच्छा चाचा के पास लगता। शाम को कभी खरबूजे कट रहे हैं, कभी चाटवाले की रेहड़ी रुकवाई जा रही है। खाने खिलाने के बेहद शौकीन हमेशा बैठक में जमघट लगा ही रहता। उस जमाने में भी सारे दिन चाय बनती रहती। इतवार को तो खास तौर से कभी मुरगा पकता, कभी पुलाव कभी केसर पड़ी रबड़ी तो कभी श्रीखंड चेहरे पर उभर आए तृषित भाव को दबाती मंजु बचपन की सुखद स्मृतियों में खो गई थी-‘रोब भी खूब था उनका उस जमाने में भी रेडियो, गद्दे लगी कुरसियाँ, फूलदार परदे और सफाई के तो बेहद कायल...
‘और सुनाइए, कैसे आना हुआ ?’ वे अंदर सबको खबर करके आकर बैठते हुए बोले।
‘जी, एक सरकारी काम के सिलसिले में आया था। मंजु ने कहा था कि बिना आपसे मिले...’
‘हाँ, हाँ, और क्या ! अच्छा, कैसी है मंजु बेटी ? उसे भी लाए होते !’
‘जी, आना तो बहुत चाहती थी, पर छोटे बच्चे के साथ जरा...’
सचमुच मंजु का आने का बहुत मन था। उसने तरह-तरह से मुझसे मनवाने की कोशिश की थी-‘सुनो, तुम्हारी गाँठ से कुछ नहीं जाएगा। रेल का टिकट तक देख लेना चाचा ही कटाएँगे और चाची साड़ी भी देंगी...कितने साल हो गए !...आठ साल पहले शादी में ही देखा है, वह भी कुछ घंटों को, उन्हें छुट्टी ही कहाँ मिली थी !...ले चलो, तुम्हें भी हाथ पर पाँच-दस देंगे ही।’
मैं झुँझला गया था। सिर से पैर तक एक हीन ग्रंथि से बाँधकर रख दिया था मंजु ने मुझे। उनके ठाट-बाट की पृष्ठभूमि के बीच वह हमारी अभावग्रसतता पर सीधा फोकस डाल रही थी।
यह मेरे अहं पर सीधी चोट थी और फिर सच कहूँ तो मुझे शादी में वे थोड़े ज्यादा ही शान दिखानेवाले और अकड़बाज लगे थे। इसी लगने की ही वजह से मैंने खुद भी उनसे ठीक से बात नहीं की थी। खुद अपनी ही शादी थी, मैं क्यों किसी से कम अकड़ता ! पर इस वक्त मंजु को अकड़कर नहीं डाँट सकता था, क्योंकि वह जो कुछ कह रही थी, सच-बेहद कड़वा यथार्थ था।
मैंने उसी सच के माध्यम से उसे समझाया, ‘ठीक है चाचा-चाची हजार दें, पर अपना भी तो कुछ फर्ज है। जहाँ जाओ, इज्जत से जाना चाहिए। चाचा-चाची के लिए न सही, उनके बच्चों के लिए तो कुछ ले ही चलना होगा-फिर अपने बच्चों के एक-आध जोड़े ठीक कपड़े....’
मंजु हताश सी चुप हो गई थी।
पर उसका दूसरा तर्क मैं नहीं काट पाया। होटल में ठहरूँगा तो ट्रैवल एलाउंस में से कुछ नहीं बचेगा। एक रात उनके यहाँ गुजारा देने से चालीस पचास रुपए का फायदा। मिठाई लेता जाऊँगा और सबसे छोटी लड़की को पाँच रुपए दे दूँगा। सो भी गलती हो गई। यहाँ आकर एक दुकान से मिठाई ली। देखने में बहुत ही कम लगी तो पूछा, ‘पाँच रुपए की है ?’
‘जी हाँ, चार सौ पचीस ग्राम।’
‘यह तो बहुत थोड़ी लग रही है!’
‘एक किलो तौल दूँ ?’ हलवाई ने बेफिक्री से पूछा।
‘नहीं-नहीं...अच्छा, ऐसा करो, इसी को जरा बड़े डिब्बे में रख दो न। डिब्बा भी तो तुम्हारा एकदम छोटा है।’ मैं झेंप मिटाने के लिए खिसियानी हँसी हँसा।
‘बड़े डिब्बे में और भी कम दिखेगी।’ उसने व्यस्तता दिखाते हुए पैने तुर्श लहजे में कहा और चलो, आगे बढ़ो’ वाली मुद्रा दिखाते हुए वही छोटा डिब्बा मेरी ओर बढ़ा दिया। डिब्बा लेते हुए मुझे चेहरे पर एक तपन-सी महसूस हुई। सारे रास्ते जब-जब हलवाई का वाक्य मन में घूमता, चेहरा फिर गरम हो उठता और मैं अपने आपको कोसता-मुझे कहना ही नहीं था, और कहा ही था तो हलवाई की बात के जवाब में कसकर कहना था, तुमसे मतलब ! कम दिखे या ज्यादा मुझे बड़े डिब्बे में ही चाहिए।
नौ दस साल की एक बच्ची रंग उड़ी छींटोंवाली धुली सी फ्रॉक पहने, बालों में अभी-अभी कंघी किए सकुचाती शरमाती आकर खड़ी हो गई।
‘मुझे जानती हो ?’
‘हूँ...’ सकुचाते-सकुचाते दोनों हाथों की मुट्ठियाँ ठोढ़ी पर लगाती बोली।
‘कौन हूँ।’
‘जीजा...जी...’
‘हो-हो-हो...’ मैंने मिठाई का डिब्बा उसे पकड़ाकर राहत की साँस ली।
डिब्बा पाते ही वह तीर की तरह भागी। अंदर शायद किसी दूसरे बच्चे ने डिब्बा छीन लिया-दोनों में लड़ाई झगड़े और फिर बच्ची के रोने की आवाज आने लगी, साथ ही किसी बड़ी जनाना आवाज का सख्त डाँट भरा स्वर। आवाजें धीमी थीं, पर साफ-साफ सुनाई पड़ रही थीं। उनके चेहरे पर आई झेंप मिटाने की गर्ज से मैंने बात शुरू की, ‘आप कैसे हैं ? शादी में जब देखा था, तब से बहुत बदल गए हैं. क्या बीमार वगैरह...’
‘नहीं, उम्र भी तो हो गई भाई, बुड्ढे हुए...हें-हें-हें-हें...’ मुझे लगा, अपनी हँसने-हँसानेवाली बात वे जबरदस्ती बरकरार रखे हुए है। पता चला दो साल का एक्सटेंशन, मिल गया, नहीं तो पचपन साल में रिटायर हो गए होते।
बाहरी दरवाजे से जरा हट सत्रह अठारह साल के एक लड़के ने उन्हें इशारे से बुलाया। वे जल्दी से उठकर गए। फिर बड़ी देर तक जेब में से पैसे निकालकर गिन-गिनाकर उसे देते, समझाते रहे। मुझे लग रहा था, उन्हीं पैसों को वे बार-बार गिन रहे हैं। बीच-बीच में लड़के का धीमा स्वर उभकता, खीझ भरा, जैसे- ‘इतने में वह कैसे आएगा ? वे फिर से बताई हुई चीज की मात्रा में कमोबेश करते, समझाते लौटकर फिर बैठ गए।
मैं खुद उनसे ज्यादा परोपेश में था। दरअसल, ऐसी नाजुक रिश्तेदारी में आना ही नहीं चाहता था, पर मंजु ने बहुत जोर डाला था, ‘चाचा को पता चलेगा तो कितना बुरा मानेंगे ! तुमने असल में उन्हें शादी पर थोड़ी ही देर को देखा है न, उनका स्वभाव नहीं जानते। बहुत ही खुशमिजाज आदमी हैं। सारा समय हँसते-हँसाते चुटकुले लतीफे सुनाते घर बाहर गुलजार किए रहते हैं। बचपन में हम सब पूरी गरमी की छुट्टियाँ चाचा के पास ही तो बिताते थे। बच्चों से उन्हें बेहद प्यार था। उनके बच्चों में तब केवल रानी थी। ओह कितना मजा आता था कभी कंधे पर बैठाकर घुमाते, कभी सब बच्चों को इकट्ठा कर ‘अकल गुम्म-अकल गुम्म’ का खेल खेलते। मैं बहुत मोटी थी न, दोनों गाल फूले रहते, सो अपना भी गाल फुलाकर ‘कुंडा लोगी कि गगरी’ कहकर चिढ़ाते उनके रहते कोई बच्चा रो नहीं सकता था। हमारी सारी जिदें पूरी की जातीं। हमें अपने घर से कहीं ज्यादा अच्छा चाचा के पास लगता। शाम को कभी खरबूजे कट रहे हैं, कभी चाटवाले की रेहड़ी रुकवाई जा रही है। खाने खिलाने के बेहद शौकीन हमेशा बैठक में जमघट लगा ही रहता। उस जमाने में भी सारे दिन चाय बनती रहती। इतवार को तो खास तौर से कभी मुरगा पकता, कभी पुलाव कभी केसर पड़ी रबड़ी तो कभी श्रीखंड चेहरे पर उभर आए तृषित भाव को दबाती मंजु बचपन की सुखद स्मृतियों में खो गई थी-‘रोब भी खूब था उनका उस जमाने में भी रेडियो, गद्दे लगी कुरसियाँ, फूलदार परदे और सफाई के तो बेहद कायल...
‘और सुनाइए, कैसे आना हुआ ?’ वे अंदर सबको खबर करके आकर बैठते हुए बोले।
‘जी, एक सरकारी काम के सिलसिले में आया था। मंजु ने कहा था कि बिना आपसे मिले...’
‘हाँ, हाँ, और क्या ! अच्छा, कैसी है मंजु बेटी ? उसे भी लाए होते !’
‘जी, आना तो बहुत चाहती थी, पर छोटे बच्चे के साथ जरा...’
सचमुच मंजु का आने का बहुत मन था। उसने तरह-तरह से मुझसे मनवाने की कोशिश की थी-‘सुनो, तुम्हारी गाँठ से कुछ नहीं जाएगा। रेल का टिकट तक देख लेना चाचा ही कटाएँगे और चाची साड़ी भी देंगी...कितने साल हो गए !...आठ साल पहले शादी में ही देखा है, वह भी कुछ घंटों को, उन्हें छुट्टी ही कहाँ मिली थी !...ले चलो, तुम्हें भी हाथ पर पाँच-दस देंगे ही।’
मैं झुँझला गया था। सिर से पैर तक एक हीन ग्रंथि से बाँधकर रख दिया था मंजु ने मुझे। उनके ठाट-बाट की पृष्ठभूमि के बीच वह हमारी अभावग्रसतता पर सीधा फोकस डाल रही थी।
यह मेरे अहं पर सीधी चोट थी और फिर सच कहूँ तो मुझे शादी में वे थोड़े ज्यादा ही शान दिखानेवाले और अकड़बाज लगे थे। इसी लगने की ही वजह से मैंने खुद भी उनसे ठीक से बात नहीं की थी। खुद अपनी ही शादी थी, मैं क्यों किसी से कम अकड़ता ! पर इस वक्त मंजु को अकड़कर नहीं डाँट सकता था, क्योंकि वह जो कुछ कह रही थी, सच-बेहद कड़वा यथार्थ था।
मैंने उसी सच के माध्यम से उसे समझाया, ‘ठीक है चाचा-चाची हजार दें, पर अपना भी तो कुछ फर्ज है। जहाँ जाओ, इज्जत से जाना चाहिए। चाचा-चाची के लिए न सही, उनके बच्चों के लिए तो कुछ ले ही चलना होगा-फिर अपने बच्चों के एक-आध जोड़े ठीक कपड़े....’
मंजु हताश सी चुप हो गई थी।
पर उसका दूसरा तर्क मैं नहीं काट पाया। होटल में ठहरूँगा तो ट्रैवल एलाउंस में से कुछ नहीं बचेगा। एक रात उनके यहाँ गुजारा देने से चालीस पचास रुपए का फायदा। मिठाई लेता जाऊँगा और सबसे छोटी लड़की को पाँच रुपए दे दूँगा। सो भी गलती हो गई। यहाँ आकर एक दुकान से मिठाई ली। देखने में बहुत ही कम लगी तो पूछा, ‘पाँच रुपए की है ?’
‘जी हाँ, चार सौ पचीस ग्राम।’
‘यह तो बहुत थोड़ी लग रही है!’
‘एक किलो तौल दूँ ?’ हलवाई ने बेफिक्री से पूछा।
‘नहीं-नहीं...अच्छा, ऐसा करो, इसी को जरा बड़े डिब्बे में रख दो न। डिब्बा भी तो तुम्हारा एकदम छोटा है।’ मैं झेंप मिटाने के लिए खिसियानी हँसी हँसा।
‘बड़े डिब्बे में और भी कम दिखेगी।’ उसने व्यस्तता दिखाते हुए पैने तुर्श लहजे में कहा और चलो, आगे बढ़ो’ वाली मुद्रा दिखाते हुए वही छोटा डिब्बा मेरी ओर बढ़ा दिया। डिब्बा लेते हुए मुझे चेहरे पर एक तपन-सी महसूस हुई। सारे रास्ते जब-जब हलवाई का वाक्य मन में घूमता, चेहरा फिर गरम हो उठता और मैं अपने आपको कोसता-मुझे कहना ही नहीं था, और कहा ही था तो हलवाई की बात के जवाब में कसकर कहना था, तुमसे मतलब ! कम दिखे या ज्यादा मुझे बड़े डिब्बे में ही चाहिए।
नौ दस साल की एक बच्ची रंग उड़ी छींटोंवाली धुली सी फ्रॉक पहने, बालों में अभी-अभी कंघी किए सकुचाती शरमाती आकर खड़ी हो गई।
‘मुझे जानती हो ?’
‘हूँ...’ सकुचाते-सकुचाते दोनों हाथों की मुट्ठियाँ ठोढ़ी पर लगाती बोली।
‘कौन हूँ।’
‘जीजा...जी...’
‘हो-हो-हो...’ मैंने मिठाई का डिब्बा उसे पकड़ाकर राहत की साँस ली।
डिब्बा पाते ही वह तीर की तरह भागी। अंदर शायद किसी दूसरे बच्चे ने डिब्बा छीन लिया-दोनों में लड़ाई झगड़े और फिर बच्ची के रोने की आवाज आने लगी, साथ ही किसी बड़ी जनाना आवाज का सख्त डाँट भरा स्वर। आवाजें धीमी थीं, पर साफ-साफ सुनाई पड़ रही थीं। उनके चेहरे पर आई झेंप मिटाने की गर्ज से मैंने बात शुरू की, ‘आप कैसे हैं ? शादी में जब देखा था, तब से बहुत बदल गए हैं. क्या बीमार वगैरह...’
‘नहीं, उम्र भी तो हो गई भाई, बुड्ढे हुए...हें-हें-हें-हें...’ मुझे लगा, अपनी हँसने-हँसानेवाली बात वे जबरदस्ती बरकरार रखे हुए है। पता चला दो साल का एक्सटेंशन, मिल गया, नहीं तो पचपन साल में रिटायर हो गए होते।
बाहरी दरवाजे से जरा हट सत्रह अठारह साल के एक लड़के ने उन्हें इशारे से बुलाया। वे जल्दी से उठकर गए। फिर बड़ी देर तक जेब में से पैसे निकालकर गिन-गिनाकर उसे देते, समझाते रहे। मुझे लग रहा था, उन्हीं पैसों को वे बार-बार गिन रहे हैं। बीच-बीच में लड़के का धीमा स्वर उभकता, खीझ भरा, जैसे- ‘इतने में वह कैसे आएगा ? वे फिर से बताई हुई चीज की मात्रा में कमोबेश करते, समझाते लौटकर फिर बैठ गए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i